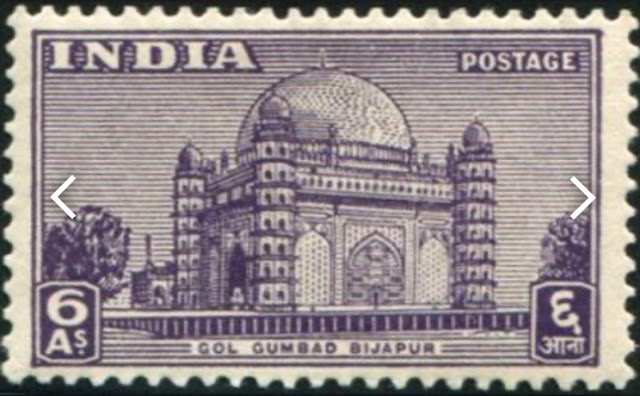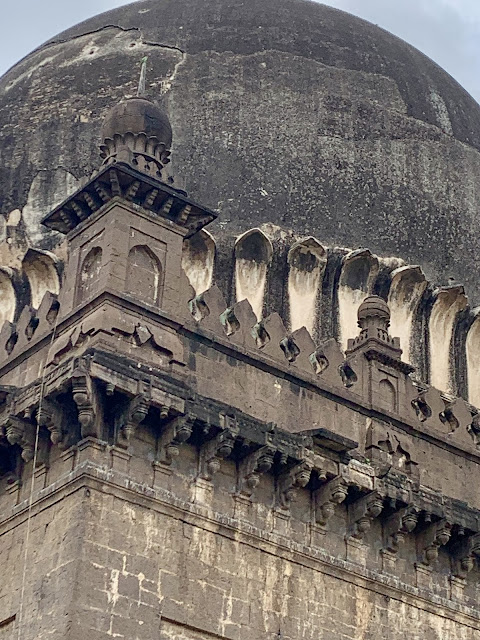अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल की तरह 2024 में 21 जून को मनाया जाएगा. इस साल योग दिवस की थीम है Yoga for Self and Society. योग ना केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी सहायक है. शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए बेजोड़ फार्मूला है जो सभी के लिए उपलब्ध है.
प्राचीन ग्रंथों में योग की कई परिभाषाएँ मिलती हैं जो मुख्य तौर पर दार्शनिक परिभाषाएँ हैं. जैसे कि
- योगश्चित्तवृतिनिरोधः अर्थात् चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है (पातंजलि योग दर्शन के अनुसार),
- पुरुषप्रकृत्योर्वियोगेपि योगइत्यमिधीयते। अर्थात् पुरुष एवं प्रकृति के पार्थक्य को स्थापित कर पुरुष का स्व स्वरूप में अवस्थित होना ही योग है( सांख्य दर्शन के अनुसार),
- योगः संयोग इत्युक्तः जीवात्म परमात्मने अर्थात् जीवात्मा तथा परमात्मा का पूर्णतया मिलन ही योग है( विष्णु पुराण के अनुसार),
- सिद्धासिद्धयो समोभूत्वा समत्वं योग उच्चते अर्थात् दुःख-सुख, लाभ-अलाभ, शत्रु-मित्र, शीत और उष्ण आदि द्वन्दों में सर्वत्र समभाव रखना योग है( भागवद्गीता के अनुसार),
- तस्माद्दयोगाययुज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् अर्थात् कर्त्तव्य कर्म बन्धक न हो, इसलिए निष्काम भावना से अनुप्रेरित होकर कर्त्तव्य करने का कौशल योग है( भागवद्गीता के अनुसार),
- मोक्खेण जोयणाओ सव्वो वि धम्म ववहारो जोगो अर्थात् मोक्ष से जोड़ने वाले सभी व्यवहार योग हैं ( जैन आचार्य हरिभद्र के अनुसार),
- कुशल चितैकग्गता योगः अर्थात् कुशल चित्त की एकाग्रता योग है( बौद्ध धर्म के अनुसार).
योग की उच्चावस्था तक पहुँचने के लिए जो साधन अपनाये गए थे उन्हीं साधनों का वर्णन योग ग्रन्थों में समय समय पर मिलता रहा है। योग की प्रामाणिक पुस्तकों में योग के चार प्रकार का वर्णन मिलता है -
1. मंत्रयोग: मंत्र योग का सम्बन्ध मन से है, मन को इस प्रकार परिभाषित किया है- मनन इति मनः। जो मनन, चिन्तन करता है वही मन है। मन की चंचलता का निरोध मंत्र के द्वारा करना मंत्रयोग है।
2 .हठयोग : हठ का शाब्दिक अर्थ हठपूर्वक किसी कार्य को करने से लिया जाता है। हठ प्रदीपिका पुस्तक में हठ का अर्थ इस प्रकार दिया है-
ह का अर्थ सूर्य तथा ठ का अर्थ चंद्र बताया गया है। सूर्य और चन्द्र की समान अवस्था हठयोग है। शरीर में कई हजार नस नाड़ियाँ है उनमें तीन प्रमुख नाड़ियों का वर्णन है, वे इस प्रकार हैं। सूर्यनाड़ी अर्थात पिंगला, चन्द्रनाड़ी अर्थात इड़ा और इन दोनों के बीच तीसरी नाड़ी सुषुम्ना है। इस प्रकार हठयोग वह क्रिया है जिसमें पिंगला और इड़ा नाड़ी के सहारे प्राण को सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करा कर समाधिस्थ किया जाता है।
3. लययोग: चित्त का अपने स्वरूप विलीन होना या चित्त की निरूद्ध अवस्था लययोग के अन्तर्गत आती है। साधक के चित्त् में जब चलते, बैठते, सोते और भोजन करते समय हर समय ब्रह्म का ध्यान रहे इसी को लययोग कहते हैं और
4. राजयोग: राजयोग सभी योगों का राजा कहलाया जाता है क्योंकि इसमें प्रत्येक प्रकार के योग की कुछ न कुछ सामग्री अवश्य मिल जाती है। राजयोग का विषय चित्तवृत्तियों का निरोध करना है।
भारतीय दर्शन में योग
मोटे तौर पर भारतीय दर्शन वेदों पर आधारित है जो लगभग 1500 ईसा पूर्व या उस से भी पहले रचे गए. वेदों की प्रभुता को मानते हुए छे दर्शन प्रसिद्द हुए हैं जिन्हें षट-दर्शन भी कहते हैं. ये हैं:
सांख्य दर्शन - जिसके प्रणेता हैं ऋषि कपिल,
योग दर्शन - जिसके प्रणेता हैं ऋषि पतंजलि,
न्याय दर्शन - जिसके प्रणेता हैं ऋषि गौतम,
वैशेषिक दर्शन - जिसके प्रणेता हैं ऋषि कणाद,
मीमांसा दर्शन - जिसके प्रणेता हैं ऋषि जैमिनी और
वेदान्त दर्शन - जिसके प्रणेता हैं ऋषि बादरायण.
इनमें से पतंजलि का योग दर्शन, सांख्य दर्शन का पूरक या व्यवहारिक दर्शन कहलाता है. इस के अपनाने से समाधी की और बढ़ा जा सकता है. इसके आठ अंग हैं:
1.यम, 2. नियम, 3. प्रत्याहार, 4. आसन, 5. प्राणायाम, 6. धारण , 7. ध्यान और 8. समाधी. इन आठ अंगों के कारण इसे अष्टांग योग भी कहा जाता है. पहले सात अंगों को अपनाते हुए आठवें पर पहुंचा जा सकता है. आज के युग में सिर्फ चौथा और पांचवां अंग मिला कर कथा समाप्त कर दी जाती है. पर चलिए आसन और प्राणायाम ही करते रहें तो कम से कम स्वास्थ्य तो सही बना रहेगा!
पतंजलि योग दर्शन में दर्शन या फलसफा तो है परन्तु योगासन, प्राणायाम या मुद्राओं का वर्णन नहीं किया गया है. आसन किस प्रकार करें या प्राणायाम कैसे करें, इसका वर्णन घेरंड संहिता में आया है.
ये किताब अंदाज़न सत्रहवीं सदी में ऋषि घेरंड द्वारा लिखी गई थी परन्तु समय के बारे में विद्वानों की राय अलग अलग है. पुस्तक संवाद के रूप में है. ऋषि घेरंड से उनका शिष्य चंड कपाली ( कहीं कहीं चंडकपालि या चण्डिका पालि भी लिखा हुआ है और कहीं कहीं पर शिष्य को राजा भी कहा गया है ), प्रश्न पूछता है और ऋषिवर उसे जवाब देते हैं. संहिता में 353 श्लोक हैं. इस पुस्तक में मनुष्य के शरीर को घट या घड़े के सामान बताया गया है जिसे योगाभ्यास के तप से शुद्ध और परिपक्व बनाया जा सकता है. घेरंड संहिता में सात अध्याय हैं. संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है -
1. षट्कर्म प्रकरण - शरीर की शुद्धि के लिए छे प्रकार के कर्म बताए गए हैं.
( i ) धौति - अंत:धौति ( वातसार धौति, वारिसार धोती, अग्निसार धौति और बहिष्कृत धौति ),
दन्त धौति ( दन्तमूल धौति, जिह्वा धौति, कर्णरन्ध्र धौति और कपालरन्ध्र धौति ),
ह्रिद्ध धौति ( दण्ड धौति, वमन धौति और वस्त्र धौति ) और मूल शोधन,
(ii). वस्ति क्रिया ( जल वस्ति और स्थल वस्ति),
(iii). नेति क्रिया ( जल नेति और सूत्र नेती ),
(iv). नौलि क्रिया ( मध्य नौलि, वाम नौलि और दक्षिण नौलि ),
(v). त्राटक क्रिया और
(vi). कपाल भाति ( वात्क्रम कपाल भाति, व्युत्क्रम कपाल भाति और शीतक्रम कपाल भाति ).
2. आसन प्रकरण - इस अध्याय में सुद्ध्र्ढ़ और निरोगी शरीर के लिए आसन बताए गए हैं. ऋषि घेरंड ने कहा है कि जितने जीव जंतु हैं उतने ही आसन हैं अर्थात चौरासी लाख. इनमें से 84 आसन श्रेष्ठ हैं और इन 84 आसनों में से 32 आसन सर्वश्रेष्ठ हैं. इन आसनों का वर्णन संहिता में है और इनके नाम इस प्रकार हैं -
1. सिद्धासन, 2. पद्मासन, 3. भद्रासन, 4. मुक्तासन, 5. वज्रासन, 6. स्वस्तिकासन, 7. सिंहासन, 8. गोमुखासन, 9. वीरासन,10. धनुरासन, 11. शवासन, 12. गुप्तासन, 13. मत्स्यासन, 14. मत्स्येन्द्रासन, 15. गोरक्षासन, 16. पश्चिमोत्तानासन, 17. उत्कट आसन, 18. संकट आसन, 19. मयूरासन, 20. कुक्कुटासन, 21. कूर्मासन, 22. उत्तानकूर्मासन, 23. मण्डुकासन, 24. उत्तान मण्डुकासन, 25. वृक्षासन, 26. गरुड़ासन, 27. वृषासन, 28. शलभासन, 29. मकरासन, 30. उष्ट्रासन, 31. भुजंगासन और 32. योगासन.
3. मुद्रा कथनम - तीसरे अध्याय में शरीर की स्थिरता बढ़ाने के लिए इन पचीस मुद्राओं का वर्णन है:
1.महामुद्रा, 2. नभोमुद्रा, 3. उड्डियान बन्ध, 4. जालन्धर बन्ध, 5. मूलबन्ध, 6. महाबंध, 7. महाबेध मुद्रा, 8. खेचरी मुद्रा, 9. विपरीतकरणी मुद्रा, 10. योनि मुद्रा, 11. वज्रोली मुद्रा, 12. शक्तिचालिनी मुद्रा, 13. तड़ागी मुद्रा, 14. माण्डुकी मुद्रा, 15. शाम्भवी मुद्रा, 16. पार्थिवी धारणा, 17. आम्भसी धारणा, 18. आग्नेयी धारणा, 19. वायवीय धारणा, 20. आकाशी धारणा, 21. अश्विनी मुद्रा, 22. पाशिनी मुद्रा, 23. काकी मुद्रा, 24. मातङ्गी मुद्रा और 25. भुजङ्गिनी मुद्रा.
4. प्रत्याहार - इस अध्याय में प्रत्याहार के विषय में बताया गया है. प्रत्याहार के पालन से इन्द्रियां अन्तर्मुखी होती हैं और धैर्य में बढ़ोतरी होती है. इन्द्रियों के बहुर्मुखी होने से साधना में विघ्न पड़ सकता है.
5. प्राणायाम - पांचवें अध्याय में शरीर के आहार और प्राणायाम की चर्चा है. शरीर को हल्का फुल्का रखने के लिए आहार का विशेष ध्यान रखना चाहिए. आहार तीन तरह का बताया गया है - मिताहार, हितकारी या गाह्य आहार और निषिद्ध या अगाह्य आहार. इनमें से मिताहार या अल्पाहार योगियों के लिए उचित माना गया है. संहिता में प्राणायाम के अभ्यास से पहले नाड़ी शोधन करने पर जोर दिया गया है. नाड़ी शोधन क्रिया से इड़ा और पिंगला में बैलेंस स्थापित होता है. संहिता में निम्न प्राणायामों का वर्णन किया गया है - 1.नाड़ी शोधन, 2. सूर्यभेदी, 3. उज्जयी, 4. शीतली, 5. भस्त्रिका, 6. भ्रामरी, 7. मूर्छा और 8. केवली.
6. ध्यानयोग - इस अध्याय में आतंरिक साक्षात्कार या प्रात्यक्षीकरण के लिए ध्यान लगाने का उल्लेख है. तीन तरह के ध्यान बताए गए हैं - स्थूल ध्यान, ज्योतिर्ध्यान और सूक्ष्म ध्यान. सर्वश्रेष्ठ ध्यान सूक्ष्म ध्यान माना गया है.
7. समाधियोग - अंतिम अध्याय में समाधि की चर्चा है. समाधी की ऊँची अवस्था में मनुष्य निर्लिप्त और अनासक्त अवस्था को प्राप्त होता है.
आजकल चलने वाले योगासन, मुद्रा, बांध, प्राणायाम का मुख्य स्रोत्र यही घेरंड संहिता है. घेरंड संहिता के कुछ समय बाद 'शिव' द्वारा 'शिव संहिता' लिखी गई. इसमें पांच अध्याय हैं और 642 श्लोक हैं जिनमें शिव-पार्वती संवाद द्वारा योग समझाया गया है. स्वात्मा राम द्वारा लिखित 'हठयोग प्रदीपिका' में भी आसन और प्राणायाम जैसी क्रियाओं का वर्णन किया गया है. यह संस्कृत में लिखी गई और इसमें चार अध्याय हैं. इनमें शारीरिक और अध्यात्मिक क्रियाओं का मिश्रण है.
ये तो थी प्राचीन काल की बात जो काफी गहराई से समझने वाली है पर इस आधुनिक युग में योगाभ्यास शारीरिक स्वास्थ्य का माध्यम है. फिर भी लगातार करते रहने से गोलियों की आवश्यकता कम पड़ती है इसमें कोई दो राय नहीं हैं. इसलिए किसी अच्छी संस्था या अच्छे गुरु से सीखें और लाभ उठाएं.
हमने भारतीय योग संस्थान, दिल्ली से 1997 में सीखी ( yogsansthan.org ) और अब तक जारी है. साल में 365 दिन तो नहीं पर हाँ 300 320 दिन से ज्यादा कर लेते हैं. अगर कहीं दूर यात्रा पर निकलते हैं तो भी योगए किट साथ ही रखते हैं. योग के साथ अगर भोजन भी संतुलित हो तो शरीर हल्का और आलस्य रहित रहता है.
कुछ आसनों की फोटो प्रस्तुत हैं.
 |
| उष्ट आसन |
 |
| कोण आसन |
 |
| गोमुख आसन |
 |
| प्राणायाम - भ्रामरी गुंजन |
 |
वृक्ष आसन
|